मैं भी 'काफ्काएस्क'
 |
| Franz Kafka |
By Gulzar Hussain
कभी-कभी सोचता हूं कि आखिर क्यों काफ्का (Franz Kafka, 3 July 1883 – 3 June 1924) ने अपने दोस्त मैक्स ब्रोड को अपनी सारी पांडुलिपियां देकर आग के हवाले कर देने को कहा होगा?
...आखिर क्यों उसके अंदर इतनी निराशा भर गई होगी? क्यों उसे लगा होगा कि उसका लिखा सब कुछ व्यर्थ है? हिटलर काल की प्रारंभिक यातनाओं- युद्ध के खतरों को नजदीक से देखने वाले एक भावुक कथाकार के अंदर कौन सी परिस्थितियां कील की तरह चुभ रही हैं, वह हर कोई जान भी तो नहीं सकता था।
क्या काफ्का का दोस्त मैक्स ब्रोड और काफ्का की प्रेमिका डोरा भी उसे ठीक से समझ पाई होगी? ..जिस डोरा की बांहों में काफ्का ने दम तोड़ा था, क्या उसने काफ्का की आंखों में झांकते वक्त उसकी बेचैनी को समझा होगा?... खैर, डोरा से ही सवाल क्यों हो, वह तो उसे महज 11 महीने पहले ही उससे मिली थी...
आजीवन बुखार में थरथराते रहे काफ्का को समझना आसान नहीं था, यह उसकी कहानियों से साफ हो जाता है, फिर भी वह जिस पीड़ा को सीने में जब्त कर कलम चला रहा था, उसे देखना जटिल होने के बावजूद नामुमकिन नहीं है। हिटलर ने जिस माइनॉरिटी धर्म को नेस्तानाबूद करने के इरादे से डेथ कैंप बनाए थे, उसी यहूदी धर्म में पैदा हुए काफ्का की कलम से जो शब्द निकल रहे थे, उन शब्दों पर दहशत की प्रतिछाया थी ...उन्हीं शब्दों में शायद वह सब कुछ झोंक देने के लिए अभिशप्त था।
उसने 1912 में मेटामॉर्फोसिस कहानी लिखी थी, जब यूरोप विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा था ...यह वही कहानी थी, जिसकी पहली पंक्ति पढ़कर मार्खेज सोचते रह गए कि आखिर कैसे एक इंसान सुबह होते ही विशालकाय कीड़े में तब्दील हो गया ...इस कहानी में सब बातें साफ हैं, लेकिन जो स्पष्ट नहीं है, वह है इस कहानी में हॉलोकॉस्ट जैसी यातना की आहट ...सत्ता के प्रताड़ना की भयावहता ...
...यह कहानी बताती है कि कैसे एक इंसान को कीड़े में बदल दिया जा सकता है। यह कहानी नरसंहार और डेथ कैंप जैसी स्थिति आने की बौद्धिक भविष्यवाणी थी ...खूनी खतरे का अलार्म थी ...काफ्का ने अपनी कलम से जो जीवन की निरर्थकता और सत्ता की भयावहता को दिखाया, उसे समझना आज भी जरूरी है ...उस अलार्म की घंटी तो अब भी मेरे कानों में सुनाई दे रही है...लेकिन ...
जर्मनी के लोगों पर काफ्का का इतना प्रभाव पड़ा था कि उन्होंने एक शब्द गढ़ा 'काफ्काएस्क' ...इसका मतलब होता है इंसान की ऐसी स्थिति, जिसमें उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखे और वो चारों ओर से मुश्किलों में घिरा हो...
कभी- कभी सोचता हूं कि क्या मैं भी 'काफ्काएस्क' (Kafkaesque) हो रहा हूं?
होलोकॉस्ट जैसे खतरे का अलार्म
काफ्का के लेखन को होलोकॉस्ट जैसे खतरे का अलार्म क्यों कहा जा सकता है?
दरअसल ऐसा सोचने के लिए हमें उसकी कहानियों में मौजूद तड़प या आत्महीनता की जद्दोजहद को समझना होगा। काफ्का की एक कहानी है ‘ए हंगर आर्टिस्ट’ (भूखा कलाकार)। इस कहानी में एक ऐसा कलाकार है जो पिंजड़े में कैद होकर 40 दिनों तक भूखा रहने की कला को प्रदर्शित करता है। लोग तालियां बजाते हैं ...कुछ लोग उपेक्षा करते हैं, लेकिन इस सीमित दिनों की सीमा से कलाकार संतुष्ट नहीं है, वह अपने मैनेजर से कहता है कि वह अभी और कई दिनों तक खुद को भूखा रखकर अपनी कला के सर्वोच्च स्तर को छूना चाहता है। अस्थिपंजर जैसी देह में तब्दील भूखे कलाकार की कहानी बेहद चौंकाने वाले अंदाज में आगे बढ़ती है।
कुछ लोग फ्रैंज काफ्का की इस कहानी को निराशावादी और एक आत्महंता का आत्मालाप मानते हैं, तो कुछ इसे काफ्का के जीवन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस कहानी में इंसानियत के घटते महत्व को दर्शाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखी गई इस कहानी का पात्र आत्महंता जरूर है, लेकिन वह आत्महंता बनने को मजबूर कर दिया गया है।
यह आदमी के टूटने की कहानी नहीं है, आदमी को सताकर उसे तोड़े जाने की कहानी है। भूख से मर रही जनता ही नहीं, उसके अलावा भी लाखों लोगों का रोजगार छीनकर क्या उसे ऐसे ही तमाशे दिखाने वाला कलाकार नहीं बना दिया जा रहा है।
बेरोजगारी के दंश से या फिर सीवर में उतरकर सफाई करने जैसे जोखिम भरे कार्यों में उतार दिये जाने को मजबूर आज के नौजवान क्या ऐसे ही मजबूर कलाकार नहीं हैं, जो लगातार मौत की ओर बढ़ रहे हैं?
काफ्का इंसानियत को मिटाने की साजिश को परत दर परत उघाड़ता है। कहानी के चरम पर जाकर भूखा कलाकार कहता है कि मुझे भी यदि मनपंसद खाना मिलता तो शायद मैं भला ऐसी स्थिति को क्यों चुनता?
गौर करने की बात है कि जर्मनी की सत्ता में हिटलर 1933 में आया था, लेकिन काफ्का ने ‘ए हंगर आर्टिस्ट’ 1922 में लिखी थी। इन दोनों समय के बीच दूरी तो है, लेकिन उतनी दूरी भी नहीं कि विश्वयुद्ध के साये में कलम चला रहा लेखक आने वाले विशाल खतरे की आहट को न पहचान सके। दरअसल सत्ता में आने से बहुत पहले ही 1920 के दशक में हिटलर इतना भयावह ढंग का करिश्माई नेता हो गया था, कि उसके पीछे सांप्रदायिक लोगों का बड़ा झुंड तैयार होने लगा था। कट्टरपंथी लोग उस पर विश्वास करने लगे थे।
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद मानवता के प्रति बढ़ते खतरे का आकलन काफ्का बखूबी कर रहा था। जर्मन भाषी साहित्यकार होने के नाते जर्मनी में पनप रहे हिटलर के खूनी-सांप्रदायिक कदम की धमक उसकी ज्यादातर कहानियों- उपन्यासों में है।
'ए हंगर आर्टिस्ट' कहानी के अंत में भूखे कलाकार की मौत हो जाती है और उसकी जगह एक जानवर को रख दिया जाता है। जानवर को किसी बात की दिक्कत नहीं है, उसे भरपूर पौष्टिक आहार दिया जाता है। कहानी की इस स्थिति से पता चलता है कि कट्टरपंथी इंसान को जानवर से कमतर समझ रहे हैं।
विश्वयुद्ध के बाद महात्वाकांक्षा की सियासत का खामियाजा कैसे आम आदमी को तड़पा सकता है, उस पल की बेचैनी को कहानियों में समेट पाने की कला काफ्का के पास थी। विश्वयुद्ध से उपजी सत्त्ता प्रेरित तड़प को जितनी शिद्दत से जर्मनी के माइनॉरिटी यहूदी महसूस कर रहे थे, उतनी ही व्याकुलता से जर्मनी से बाहर रहने वाला यहूदी काफ्का भी इसे महसूस कर रहा था।
काफ्का इन सारी स्थितियों को पन्ने पर उतारकर दुनिया को सतर्क कर रहा था...
काफ्का से आतंकित होने का मतलब
आपको याद होगा कथादेश में छपा राजेन्द्र यादव (Rajendra Yadav) का वह लंबा इंटरव्यू। उसमें वे कई विषयों को छूते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान उनके प्रिय लेखकों वाले डिसकशन पर ले जाना चाहता हूं, जहां वह फ्रैंज काफ्का सहित अन्य लेखकों के बारे में बात करते हैं। वे टॉलस्टय, दोस्तोवस्की, चेखव, ज्विग से होते हुए काफ्का तक पहुंचते हैं।
वे काफ्का के बारे में कहते हैं-''काफ्का से जरूर मैं बहुत दिनों तक आतंकित रहा। शायद आज भी हूं।''
मैं भी राजेन्द्र यादव की तरह ही काफ्का से आतंकित हूं। हां, 'आतंकित होना' ही सबसे उचित शब्द है काफ्का के रचना संसार को व्याख्यायित करने के लिए। मैं भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए काफ्का की कहानियों को इमीटेट कर सकता हूं। काफ्का की कहानियां हमें आतंकित करती हैं, ताकि हम किसी क्रूर सत्ता या हिंसक संगठन के आतंक को पहचान पाएं और रास्ता तय करें।
जरा सोचिए, काफ्का की एक कहानी (मेटामोरफॉसिस) का मुख्य पात्र सुबह जब उठता है तो वह एक विशालकाय कीड़े में बदल गया है। सोचिए कि यह क्या है। उसके कीड़े में बदलते ही उसके सारे अपने, जिनके लिए उसने सारे सपने चुने थे, वे ही उसे दुत्कारते हैं। उससे सबसे अधिक प्यार करने वाला पिता उस पर एक सड़े सेब से निशाना साधता है, जो उसकी पीठ में धंस जाता है। यह आत्मधिक्कार की कैसी स्थिति है, जिसमें एक इंसान फेंक दिया गया है। यह हमें आतंकित ही तो कर सकता है।
यह है काफ्का का महत्व कि वह हमें 'शांत' नहीं करता बेचैन करता है। उसकी कहानी (ए हंगर आर्टिस्ट) का एक पात्र अपने भूखे रहने की कला के चरम पर पहुंच कर लोगों की प्रशंसा पाना चाहता है। आखिर उसे क्या हो गया है कि वह एक पिंजड़े में भूंसे पर बैठकर भूख की चरम अवस्था को छूने को अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बना चुका है।
काफ्का के रचना संसार को निराशावादी धुंध समझकर देखना, उससे मुंह फेर लेना होगा।
दरअसल इंसान को जो सब ह्युमन बनाकर उसे हाशिए पर धकेल देने की साजिश रची गई या रची जा रही है, वह काफ्का के लेखन की धुरी था। वह अपने समय और उससे आगे के खतरों के बारे में आगाह कर रहा था और कर रहा है।
वह रेखाओं के माध्यम से भी मानवीय पीड़ा को व्यक्त कर रहा था
प्रथम विश्व युद्ध के खतरों से आहत काफ्का का संवेदनशील मन केवल लेखन से संतुष्ट नहीं था, वह रेखाओं के माध्यम से भी मानवीय पीड़ा को व्यक्त कर रहा था।
...शायद लिखने से पहले वह उस स्थिति को लेकर जो सोचता था, वही उसके रेखांकन का अंकुर था ...शायद उसके मन में त्रासदी के बीच टूटता और आकार लेता मानव एक छवि चाहता था, जो रेखांकन के बाद और स्पष्ट होता जाता था।
किसी चित्र में भविष्य के भयानक खतरों को लेकर चिंतित आदमी दिखाई देता था, तो किसी में कोई राह नहीं सूझने पर व्यथित हुआ इंसान दिखाई देता था।
काफ्का मानव के दुखों का अदभुत चितेरा था, जो कहानियों से जितना चौंकाता था, उतना ही अपने रेखांकनों के माध्यम से आपको बेचैन कर देता था।
काफ्का को यह पता था कि जब वह जला देने के लिए अपने दोस्त मैक्स ब्रोड को पांडुलिपियां सौंपेगा, तो उसकी डायरी के पन्नों पर उगे चित्र भी जल जाएंगे ...लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया ...काफ्का चाहता तो खुद ही अपनी रचनाओं को जला देता, फिर उसने अपने दोस्त को यह जलाने का कार्य क्यों सौंपा? क्या उसके मन के किसी कोने में यह बात थी कि मैक्स उसके तकलीफ भरे लेखन को बचा लेगा...खैर, ठीक-ठीक तो काफ्का ही जानता था कि वह क्या चाहता था, लेकिन उसके रेखांकन को देखकर आप कुछ समझ सकते हैं, तो समझिए ...
...वह बेचैनी ...वह तड़प ...वह दुनिया को बेहतर बनाने की अकांक्षा...
...यह केवल उसी के लिए तो नहीं थी, आपके लिए भी थी ...
काफ्का और मंटो: दोनों की कहानियों में एक सी चीख
मैं मंटो (Saadat Hasan Manto) और काफ्का को एक डोर से जोड़ने का इच्छुक हूं। अब, आप पूछेंगे कि दोनों में समानता क्या लगी आपको? तो मैं सीधे-सीधे यह कहूंगा कि एक ने विश्वयुद्ध के साये में लिखा और दूसरे ने भारत के बंटवारे के दौरान उपजे मानवीय दर्द को अपने सीने में जब्त किया। दोनों ने अपनी कलम से बेइंतहा दर्द को सामने लाया। दोनों की कहानियों में यातना से दबकर टूटते इंसान की चीख है। दोनों की कहानियों में एक सी चीख है।
काफ्का और मंटो को जितना पढ़ा है, उसी आधार पर आपको कुछ बताना चाहता हूं। काफ्का की कहानियों में जो बेचैनी है, तड़प है और भयावहता है, वह मंटो की कहानियों में नहीं है, लेकिन मंटों अपने जर्द चेहरों वाले पात्रों से क्या कहलवाना चाहता है, उस पर गौर कीजिए।
एक तरफ काफ्का की कहानी 'दंडद्वीप' में सजा दिए जाने का खौफनाक वर्णन है, तो दूसरी ओर मंटो की ‘खोल दो’ जैसी कहानी में सांप्रदायिकता से उपजा वहशीपन है। आखिर यह सब क्या है?
दोनों साहित्यकार खून उगलते हुए मरे। तपेदिक से तो मरे, यह तो कहने की बात है, दरअसल उन्हें ऐसे मरने को स्थितियों ने मजबूर किया। वे वैसे नहीं मरते तो भी मारे जाते। वे देख रहे थे खुली आंखों से यातनाओं के दौर को... छल और फरेब को ...
उन दोनों को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन पढ़िए उन्हें... उन दोनों ने अपने सामने तड़पते लोगों को देखा ...गम में छटपटाते लोगों को देखा।
इस तरह की त्रासदी के दौर में ये ऐसे न लिखते, तो कैसे लिखते?




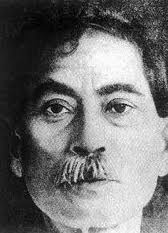
Comments
Post a Comment