प्रेमचंद के साहित्य में कैसे हैं गाँव -देहात ?
- गुलज़ार हुसैन
कहानी और उपन्यास की दुनिया भले ही प्रेमचंद युग से काफी आगे निकल गई है ...बहुत बदल भी गई है, लेकिन प्रेमचंद अब भी प्रासंगिक हैं। गरीब किसानों,मजदूरों और गांवों के दबे-कुचले लोगों के दुख -दर्द को जितनी गहराई से प्रेमचंद ने उठाया,उस तरह उनके समकालीन और उनके बाद के साहित्यकार नहीं उठा सके। सच तो यह भी है कि प्रेमचंद के नक्शे-कदम पर चलने वाले साहित्यकार भी उनकी लेखनी सा प्रभाव और जनप्रिय शैली नहीं पा सके। गरीब किसानों की समस्या को समझने और गांवों में दलितों -पिछड़ों के दैनिक संघर्षों को बेहद संवेदनात्मक तरीके से उजागर करने की अद्भुत कला प्रेमचंद के पास थी। वे खेतिहर मजदूरों के संघर्षों के साथ ही उनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को भी बड़ी गहराई से चित्रित करते थे। उनके पात्र इतने जीवंत होते थे कि पाठक उनके दुखों- सुखों से खुद को आसानी से जोड़ पाते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनका कालजयी उपन्यास 'गोदान' है। 'गोदान' का मुख्य पात्र होरी हिंदी साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य में परिचित नाम है। होरी के बहाने प्रेमचंद ने भारतीय गरीब किसान के जीवन की सबसे दर्दनाक कहानी लोगों के सामने रखी। दरअसल प्रेमचंद ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले गरीब किसानों और पिछड़ों -दलितों की जो स्थिति देखी थी,उससे उन्होंने यह भांप लिया था कि आने वाले समय में खेतीबारी करनेवाले मजदूरों को सबसे बड़ी समस्याओं से दो -चार होना पड़ेगा। किसानों के बारे में प्रेमचंद के साहित्यिक और गैर साहित्यिक रचनाओं में जो विचार मिलते हैं वे वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। वे अपनी लेखनी से न केवल वर्तमान
बल्कि भविष्य को भी देख-समझ पा रहे थे।
प्रेमचंद के शुरुआती लेखन में गांधीवाद का जबर्दस्त प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन वे अपनी रचनाओं का अंतिम सत्य या चरमोत्कर्ष गांधीवादी नजरिए से नहीं तौलते हैं। बाद में धीरे- धीरे उनके साहित्य में गांधीवाद से मोहभंग देखने को मिलता है। गोदान तक आते -आते उनमें साम्यवाद और भारत में पनप रहे आंबेडकरवाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन उनकी रचनाओं की विशेषता यही रही है कि वे किसी भी वाद के प्रभाव से अपनी लेखन शैली को बोझिल नहीं होने देते हैं। अंततःउनके साहित्य में गहराई तक पैठ मानवीय छटपटाहटों -संवेदनाओं का ही है। उन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज में अपनी अवाज मिलाने की कोशिश की है। प्रेमचंद के समकालीन साहित्यकार मैक्सिम गोर्की भी ऐसी ही पीड़ा को स्वर दे रहे थे। निस्संदेह मार्क्सवाद उस दौर में युवाओं को सबसे अधिक प्रभावित भी कर पा रहा था और प्रेमंचद ने अपने अंतिम दिनों में वहां से रचनाओं के लिए बहुत सारी ऊर्जा ली थी।
प्रेमचंद को गांवों -देहातों का चितेरा भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में गांवों का जो रूप आया है वह सचमुच अनोखा है। वह गांव के सौंदर्य को वहां रहने वाली गरीब जनता के दर्द से जोड़ देते हैं। वह गांवों में कलकल बहती नदी को देखते हैं, तो उसके किनारे खेतों में जी-तोड़ मेहनत कर रहे खेतिहर मजदूर को भी देखते हैं। वे रोटी खाने के लिए बहने वाले पसीने को ओस की बूंद से अधिक महत्व देते रहे हैं। हां ,वे गांव के चितेरे हैं,लेकिन उन्होंने गांव में रह कर वहां के कष्टों को देखा हैं। उनकी दृष्टि में गांव में रहने वाले 'होरी', 'गोबर' और 'सीलिया' के दुख-दर्द छुपे हैं। वे अपनी रचनाओं में अगर गांव रचते हैं, तो वहां के 'विलेन' भूमिपतियों -जमींदारों के शोषण के हथियारों को भी देखते हैं। सच,उनकी रचनाओं में गांवों-देहातों का सबसे कष्टप्रद वर्णन हैं। एक तरह से उनके साहित्य में गांवों को शोषण का सबसे बड़ा क्षेत्र ही समझा गया है।
'कफन','सद्गति','पूस की रात' सहित उनकी कई कहानियों में गांव का रूप सुंदर नहीं असुंदर है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि वे गांवों -देहातों को अपने स्तर पर तौलते प्रतीत होते हैं। 'गोदान' में होरी का बेटा गोबर गांव से दूर भागना चाहता है। वह शहर जाना चाहता है। गोबर शहर जाता भी है, लेकिन उसकी स्थिति वहां और भी दयनीय हो जाती है। प्रेमचंद ने गांवों और शहरों दोनों जगहों पर गरीबों के लिए खड़ी दमनकारी व्यवस्था को दिखाने का प्रयास किया। प्रेमचंद ने 'निर्मला','रंगभूमि' और 'कर्मभूमि' सहित कई अन्य उपन्यासों में उस समय की सबसे बड़ी समस्याओं को छूआ। 'निर्मला' में उन्होंने स्त्री के अंतर्द्वंद्व और पुरुषवादी समाज के शंकालु चरित्र को बड़ी ही गहराई से प्रस्तुत किया है। स्त्री और दलितों को उन्होंने उस समय अपने साहित्य में स्थान दिया,जब अन्य साहित्यकार इन विषयों पर लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 'सद्गति' और 'कफन ' में उन्होंने दलितों के जीवनयापन और उनके साथ जुड़ी त्रासदी को सामने रखा है। इन कहानियों में पाखंडी धनपतियों का दोहरा चरित्र लोगों को चौंकाता है। वे इन कहानियों से यह भी बताते हैं कि उस समय दलितों पर कितने भीषण अत्याचार हो रहे थे।
३१ जुलाई,१८८० को वाराणसी के निकट लमही में जन्में प्रेमचंद का रहन-सहन बहुत सामान्य था, लेकिन गरीबी का दंश उनकी लेखनी की धार को नहीं रोक पाया। वे गरीबों-दलितों के बीच रह कर उनके संघर्षों के लिए लड़ रहे थे। वे फिल्मों में कहानियां लिखने मुंबई भी आए,लेकिन मुंबई फिल्मी दुनिया से उनका जल्द ही मोहभंग हो गया। वे उस दौर में पूंजीवादियों से घिरे फिल्मी दुनिया से ऊब गए। उनको लगा कि ऐसे माहौल में रहकर वे स्तरीय लेखन नहीं कर पाएंगे। वे मुंबई से लौट गए। पैसे की तंगी के बावजूद वे अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन करते रहे। परिपूर्णानंद वर्मा ने अपने संस्मरणात्मक पुस्तक 'बीती यादें ' में उनके बारे में बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि कई बार प्रेमचंद फाउंटेन पेन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। वे स्याही में निब डूबो कर लिखते थे। वर्मा ने एक बार उन्हें रद्दी से खरीद कर लाए एक तरफ पहले से लिखे कागज पर लिखते देखा तो पूछा कि आप सफेद पेपर पर फाउंटेन पेन से क्यों नहीं लिखते? तब प्रेमचंद ने मुस्काते हुए उत्तर दिया कि ज्यादा अमीरी ढंग से लिखूंगा तो क्या लेखन में अमीरी नहीं आ जाएगी? मुझे तो ऐसे ही लिखने में आनंद आता है। तो ऐसे थे प्रेमचंद। गरीबी में लिखते -लिखते ही उनका देहांत १९३६ में हो गया। अंत समय तक उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। अस्वस्थ होने पर वे कहते थे कि मैं मजदूर हूं,जिस दिन नहीं लिखूंगा उस दिन खाने का अधिकार भी मुझे नहीं है। सचमुच, उनकी लेखनी का महत्व कभी भी कम नहीं होगा।
कहानी और उपन्यास की दुनिया भले ही प्रेमचंद युग से काफी आगे निकल गई है ...बहुत बदल भी गई है, लेकिन प्रेमचंद अब भी प्रासंगिक हैं। गरीब किसानों,मजदूरों और गांवों के दबे-कुचले लोगों के दुख -दर्द को जितनी गहराई से प्रेमचंद ने उठाया,उस तरह उनके समकालीन और उनके बाद के साहित्यकार नहीं उठा सके। सच तो यह भी है कि प्रेमचंद के नक्शे-कदम पर चलने वाले साहित्यकार भी उनकी लेखनी सा प्रभाव और जनप्रिय शैली नहीं पा सके। गरीब किसानों की समस्या को समझने और गांवों में दलितों -पिछड़ों के दैनिक संघर्षों को बेहद संवेदनात्मक तरीके से उजागर करने की अद्भुत कला प्रेमचंद के पास थी। वे खेतिहर मजदूरों के संघर्षों के साथ ही उनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को भी बड़ी गहराई से चित्रित करते थे। उनके पात्र इतने जीवंत होते थे कि पाठक उनके दुखों- सुखों से खुद को आसानी से जोड़ पाते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनका कालजयी उपन्यास 'गोदान' है। 'गोदान' का मुख्य पात्र होरी हिंदी साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य में परिचित नाम है। होरी के बहाने प्रेमचंद ने भारतीय गरीब किसान के जीवन की सबसे दर्दनाक कहानी लोगों के सामने रखी। दरअसल प्रेमचंद ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले गरीब किसानों और पिछड़ों -दलितों की जो स्थिति देखी थी,उससे उन्होंने यह भांप लिया था कि आने वाले समय में खेतीबारी करनेवाले मजदूरों को सबसे बड़ी समस्याओं से दो -चार होना पड़ेगा। किसानों के बारे में प्रेमचंद के साहित्यिक और गैर साहित्यिक रचनाओं में जो विचार मिलते हैं वे वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। वे अपनी लेखनी से न केवल वर्तमान
बल्कि भविष्य को भी देख-समझ पा रहे थे।
प्रेमचंद के शुरुआती लेखन में गांधीवाद का जबर्दस्त प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन वे अपनी रचनाओं का अंतिम सत्य या चरमोत्कर्ष गांधीवादी नजरिए से नहीं तौलते हैं। बाद में धीरे- धीरे उनके साहित्य में गांधीवाद से मोहभंग देखने को मिलता है। गोदान तक आते -आते उनमें साम्यवाद और भारत में पनप रहे आंबेडकरवाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन उनकी रचनाओं की विशेषता यही रही है कि वे किसी भी वाद के प्रभाव से अपनी लेखन शैली को बोझिल नहीं होने देते हैं। अंततःउनके साहित्य में गहराई तक पैठ मानवीय छटपटाहटों -संवेदनाओं का ही है। उन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज में अपनी अवाज मिलाने की कोशिश की है। प्रेमचंद के समकालीन साहित्यकार मैक्सिम गोर्की भी ऐसी ही पीड़ा को स्वर दे रहे थे। निस्संदेह मार्क्सवाद उस दौर में युवाओं को सबसे अधिक प्रभावित भी कर पा रहा था और प्रेमंचद ने अपने अंतिम दिनों में वहां से रचनाओं के लिए बहुत सारी ऊर्जा ली थी।
प्रेमचंद को गांवों -देहातों का चितेरा भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में गांवों का जो रूप आया है वह सचमुच अनोखा है। वह गांव के सौंदर्य को वहां रहने वाली गरीब जनता के दर्द से जोड़ देते हैं। वह गांवों में कलकल बहती नदी को देखते हैं, तो उसके किनारे खेतों में जी-तोड़ मेहनत कर रहे खेतिहर मजदूर को भी देखते हैं। वे रोटी खाने के लिए बहने वाले पसीने को ओस की बूंद से अधिक महत्व देते रहे हैं। हां ,वे गांव के चितेरे हैं,लेकिन उन्होंने गांव में रह कर वहां के कष्टों को देखा हैं। उनकी दृष्टि में गांव में रहने वाले 'होरी', 'गोबर' और 'सीलिया' के दुख-दर्द छुपे हैं। वे अपनी रचनाओं में अगर गांव रचते हैं, तो वहां के 'विलेन' भूमिपतियों -जमींदारों के शोषण के हथियारों को भी देखते हैं। सच,उनकी रचनाओं में गांवों-देहातों का सबसे कष्टप्रद वर्णन हैं। एक तरह से उनके साहित्य में गांवों को शोषण का सबसे बड़ा क्षेत्र ही समझा गया है।
'कफन','सद्गति','पूस की रात' सहित उनकी कई कहानियों में गांव का रूप सुंदर नहीं असुंदर है। प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि वे गांवों -देहातों को अपने स्तर पर तौलते प्रतीत होते हैं। 'गोदान' में होरी का बेटा गोबर गांव से दूर भागना चाहता है। वह शहर जाना चाहता है। गोबर शहर जाता भी है, लेकिन उसकी स्थिति वहां और भी दयनीय हो जाती है। प्रेमचंद ने गांवों और शहरों दोनों जगहों पर गरीबों के लिए खड़ी दमनकारी व्यवस्था को दिखाने का प्रयास किया। प्रेमचंद ने 'निर्मला','रंगभूमि' और 'कर्मभूमि' सहित कई अन्य उपन्यासों में उस समय की सबसे बड़ी समस्याओं को छूआ। 'निर्मला' में उन्होंने स्त्री के अंतर्द्वंद्व और पुरुषवादी समाज के शंकालु चरित्र को बड़ी ही गहराई से प्रस्तुत किया है। स्त्री और दलितों को उन्होंने उस समय अपने साहित्य में स्थान दिया,जब अन्य साहित्यकार इन विषयों पर लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 'सद्गति' और 'कफन ' में उन्होंने दलितों के जीवनयापन और उनके साथ जुड़ी त्रासदी को सामने रखा है। इन कहानियों में पाखंडी धनपतियों का दोहरा चरित्र लोगों को चौंकाता है। वे इन कहानियों से यह भी बताते हैं कि उस समय दलितों पर कितने भीषण अत्याचार हो रहे थे।
३१ जुलाई,१८८० को वाराणसी के निकट लमही में जन्में प्रेमचंद का रहन-सहन बहुत सामान्य था, लेकिन गरीबी का दंश उनकी लेखनी की धार को नहीं रोक पाया। वे गरीबों-दलितों के बीच रह कर उनके संघर्षों के लिए लड़ रहे थे। वे फिल्मों में कहानियां लिखने मुंबई भी आए,लेकिन मुंबई फिल्मी दुनिया से उनका जल्द ही मोहभंग हो गया। वे उस दौर में पूंजीवादियों से घिरे फिल्मी दुनिया से ऊब गए। उनको लगा कि ऐसे माहौल में रहकर वे स्तरीय लेखन नहीं कर पाएंगे। वे मुंबई से लौट गए। पैसे की तंगी के बावजूद वे अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ लेखन करते रहे। परिपूर्णानंद वर्मा ने अपने संस्मरणात्मक पुस्तक 'बीती यादें ' में उनके बारे में बहुत सारे अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि कई बार प्रेमचंद फाउंटेन पेन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। वे स्याही में निब डूबो कर लिखते थे। वर्मा ने एक बार उन्हें रद्दी से खरीद कर लाए एक तरफ पहले से लिखे कागज पर लिखते देखा तो पूछा कि आप सफेद पेपर पर फाउंटेन पेन से क्यों नहीं लिखते? तब प्रेमचंद ने मुस्काते हुए उत्तर दिया कि ज्यादा अमीरी ढंग से लिखूंगा तो क्या लेखन में अमीरी नहीं आ जाएगी? मुझे तो ऐसे ही लिखने में आनंद आता है। तो ऐसे थे प्रेमचंद। गरीबी में लिखते -लिखते ही उनका देहांत १९३६ में हो गया। अंत समय तक उन्होंने लिखना बंद नहीं किया। अस्वस्थ होने पर वे कहते थे कि मैं मजदूर हूं,जिस दिन नहीं लिखूंगा उस दिन खाने का अधिकार भी मुझे नहीं है। सचमुच, उनकी लेखनी का महत्व कभी भी कम नहीं होगा।
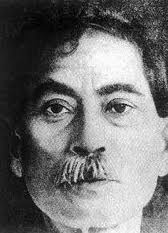



प्रेमचन्द जी बेहद ही संवेदनशील इन्सान थे और उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के जातिवाद, महिलाओं के शोषण,खास भारत के गांवों की ज़मीनी हकीकत समाज के सामने रखी । आजादी के दौरान सोजे वतन,कफ़न जैसा साहित्य सच में प्रेमचंद जी ही लिख सकते थे अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ भुगता लेकिन केवल उस को ही सार्थक न मानकर बल्कि एक विज्ञानिक दृष्टि कोण अपनाते हुए समाज की समिक्षा की। पुरुष और महिला के संदर्भ में उन्होंने कहा भी है कि पुरुष को इन्सान केवल एक महिला ही बनाती है वरना वह पशु समान है। महिलाओं के गुण, प्रेम, संवेदनशीलता , त्याग, सेवा भाव , परोपकार जो महिलाओं में हैं वो कहीं नहीं मिलते । प्रेमचंद जी का साहित्य आज भी समाज को समझने और उस की समीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भुमिका निभा रहा है। चाहे मजदूर वर्ग हो,या चाहे किसान कोई भी पहलू उन की कलम से अछूता नहीं है। ये दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी।आज भी वो मौजूद हैं।
ReplyDelete