मेहनतकश की बस्तियों में बसी है मुंबई की जान
कभी फिल्म वालों ने इसे प्रसिद्ध बनाने का दावा किया, तो कभी चित्रकारों-साहित्यकारों ने इसकी नींव मजबूत करने का दावा किया। दावे लाखों किए गए, लेकिन मुंबई ने इन दावों से प्रभावित हुए बिना ही सब को समान रूप से सीने से लगाया और प्यार दिया। मुंबई ने कभी किसी प्रांत विशेष, भाषा विशेष, धर्म या जाति विशेष के नाम से प्रभावित होकर स्नेह नहीं दिया, बल्कि जी जान लगाकर मेहनत करने और संघर्ष करने वालों को ही अपना बनाया।
 |
| Photo by Gulzar Hussain |
जाने क्या बात है बंबई तेरी शबिस्तां में
हम शाम-ए-अवध, सुबह-ए-बनारस छोड़ आए हैं
- अली सरदार जाफरी
‘मुंबई महानगर’ (Mumbai) कभी शायरों और मजदूरों के होठों पर ‘क्रांति गीत’ बनकर थिरकने वाला शहर कहलाया, तो कभी यह राजनीति की भट्ठी में तपकर चर्चा में रहने वाला महानगर बना, लेकिन इसकी रवानगी को बदल पाना कभी किसी के बस में नहीं रहा।
इस महानगर को सबने अपने-अपने नजरिए से देखा। मराठियों ने इसे अपना शहर माना, तो उत्तर भारतीयों ने अपनी मेहनत से इस शहर को सजाने संवारने का दावा किया। कभी गुजरातियों, तो कभी मारवाड़ियों ने अपने व्यापार से इस शहर को चमकाने का दावा किया और कभी दक्षिण भारतीयों और बंगालियों ने इसे सांस्कृतिक रूप से स्तरीय बनाने का दावा किया। कभी फिल्म वालों ने इसे प्रसिद्ध बनाने का दावा किया, तो कभी चित्रकारों-साहित्यकारों ने इसकी नींव मजबूत करने का दावा किया। दावे लाखों किए गए, लेकिन मुंबई ने इन दावों से प्रभावित हुए बिना ही सब को समान रूप से सीने से लगाया और प्यार दिया। मुंबई ने कभी किसी प्रांत विशेष, भाषा विशेष, धर्म या जाति विशेष के नाम से प्रभावित होकर स्नेह नहीं दिया, बल्कि जी जान लगाकर मेहनत करने और संघर्ष करने वालों को ही अपना बनाया।
यह सच है कि मुंबई को देश के कोने- कोने से आए लोगों ने अपनी संस्कृति और रचनात्मक शैली से सजाया- संवारा है। हमारे देश के ग्रामीण, कस्बाई और पहाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य की खुशबू मुंबई में रची बसी है। यहां की फिल्मों के अलावा रंगमंच और अन्य साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में मुंबई की इस विविधता के सौंदर्य को देखा और महसूस किया जा सकता है।
मेहनत करने वालों ने सही रूप में मुंबई की नींव को मजबूत किया है। इनके पसीने के बल पर यहां की आकाश छूती इमारतें, मॉल, बिजनेस हब या समंदर के किनारे पसरा मतस्य उद्योग दुनिया के सामने अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेहनत-मजदूरी करने वालों ने अपने कंधे पर मुंबई को टिकाए रखा है।मुंबई जैसे विशाल महानगर को अपने पसीने से सींचने वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों, ठेलेवालों, डब्बावालों, मछुआरों और अन्य छोटे-छोटे धंधे करनेवालों, कारीगरों का यहां के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन मेहनत करने वालों ने सही रूप में मुंबई की नींव को मजबूत किया है। इनके पसीने के बल पर यहां की आकाश छूती इमारतें, मॉल, बिजनेस हब या समंदर के किनारे पसरा मतस्य उद्योग दुनिया के सामने अपना एक विशेष स्थान बनाए हुए है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मेहनत-मजदूरी करने वालों ने अपने कंधे पर मुंबई को टिकाए रखा है।
दरअसल, मुंबई और उसके उपनगरों में छोटे बड़े उद्योगों और कारखानों का एक जाल सा बिछा है,जो बीमारू प्रदेशों के लोगों को रोजगार पाने के लिए आकर्षित करता है। यहां बैग-पर्स, खिलौने, जींस पैंट-शर्ट और कई चीजों को बनाने के कारखाने हैं जहां दूर-दराज के लोग आकर दिन-रात मेहनत करते हैं।मुंबई में ऐसे तो देश के हर क्षेत्र से लोग आते हैं, लेकिन अधिकांश मेहनतकश लोग उत्तर भारत से आते हैं। बिहार (Bihar), उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल से भी लोग यहां काम करने के लिए आते हैं। मजदूरी और छोटे-छोटे कार्य करने के लिए अधिकांश लोग हिंदी पट्टी से आते हैं। मुंबई और उसके उपनगरों में इमारतों के निर्माण कार्यों में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा यहां की फिल्म इंडस्ट्री में भी कई तरह के मेहनत-मशक्कत का काम करने वाले लगे रहते हैं। दरअसल, मुंबई और उसके उपनगरों में छोटे बड़े उद्योगों और कारखानों का एक जाल सा बिछा है,जो बीमारू प्रदेशों के लोगों को रोजगार पाने के लिए आकर्षित करता है। यहां बैग-पर्स, खिलौने, जींस पैंट-शर्ट और कई चीजों को बनाने के कारखाने हैं जहां दूर-दराज के लोग आकर दिन-रात मेहनत करते हैं।
गौरतलब है कि 80 के दशक में जब मिल मजदूरों की हड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ, तब मुंबई के मेहनतकशों में एक बड़े परिवर्तन को रेखांकित किया जाने लगा। 1982 में ट्रेड यूनियन नेता दत्ता सामंत के नेतृत्व में हुए टेक्सटाइल स्ट्राइक का ऐतिहासिक महत्व रहा है। इस दौरान 25 लाख से अधिक मजदूरों ने इसमें हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया था कि मुंबई की सांस मजदूरों के बल पर चलती है। दरअसल इससे पहले तक मुंबई के मिल मजदूरों का उल्लेखनीय दौर था। उसके बाद धीरे-धीरे कपड़ा मिलों में हड़ताल और आंदोलनों का दौर आया। मजदूर यूनियनों के आंदोलन से मुंबई में पूंजीपतियों के साथ मजदूरों की टकराहट को लोग रेखांकित करने लगे। फिल्मों और साहित्य में इसका खूब प्रभाव देखा गया। जितेंद्र भाटिया ने अपनी कहानियों में मजदूरों की व्यथा का बहुत शिद्दत से उल्लेख किया। फिल्मों और रंगमंच में भी मजदूर अपनी आवाज बुलंद करते हुए उपस्थित हुए।
आखिरकार फिल्म बनकर पूरी हुई, लेकिन रिलीज होने से पहले ही बहुत बवाल हो गया। दरअसल, सेंसर बोर्ड का एक सदस्य पूंजीपतियों और मिल मालिकों के एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ था और उसको इस फिल्म के कई दृश्य चुभ गए। वह फिल्म देखने के बाद बौखला गया और इसे पूंजीपति विरोधी कहकर रिलीज होने से रोक दिया।स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की मुंबई (तब बंबई) में मजदूरों की समस्याओं और उनकी विवशता को समझने के लिए साहित्यकार प्र्रेमचंद (Premchand) से जुड़े एक घटनाक्रम का यहां उल्लेख किया जाना जरूरी है। वर्ष 1934 में प्रेमचंद ने मुंबई आकर फिल्मों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। वे तब अजंता सिनेटोन के लिए पटकथाएं लिख रहे थे। उसी दौर में प्रेमचंद की एक कहानी ‘मजदूर’ पर फिल्म बनाने की शुरुआत हुई थी।
 |
| वर्ष 1934 में प्रेमचंद ने मुंबई आकर फिल्मों के लिए लिखना शुरू कर दिया था। उसी दौर में प्रेमचंद की एक कहानी ‘मजदूर’ पर फिल्म बनाने की शुरुआत हुई थी। |
मुंबई के गीतकारों और शायरों ने अपनी कलम से मजदूरों की समस्या को बखूबी उजागर किया। साहिर लुधियानवी ने लिखा-
‘‘ आज से ऐ मजदूर-किसानों! मेरे राग तुम्हारे हैं
फाकाकश इंसानों! मेरे जोग-बिहाग तुम्हारे हैं। ’’
साहिर के अलावा अली सरदार जाफरी, मंटो की रचनाओं में भी मुंबई के मेहनतकश लोगों की जिंदगी का दर्द बखूबी उकेरा गया है। मंटो ने तो मुंबई की संघर्ष भरी जिंदगी जीने वालों पर जो कहानियां लिखीं, वे अमर हो गर्इं।
मुंबई की वेश्याओं और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी को जगदंबाप्रसाद दीक्षित ने अपने उपन्यास ‘मुर्दाघर’में बहुत गहराई से सामने रखा है। उन्होंने अपने उपन्यास के बहाने बशीरन और जब्बार जैसे कई पात्रों को अमर कर दिया। इस उपन्यास का एक अंश देखिए- ‘‘ हंसती है बशीरन। ...कितना भाई है तेरा मुंबई में? - आक्खा मुंबई का लोक मेरा भाई है। जो साब कू देंगा रुपिया...वोच मेरा भाई हो जाएंगा। भाई नई होएंगा, तो बाप हो जाएंगा। बाप नई होएंगा तो मरद हो जाएंगा। साला ये लोग कितना पइसा कमाता! उधर होम का छोकरी लोग भूका मरता। इसकी मां की...’’
रचनाकारों ने मुंबई के फुटपाथों, प्लेटफार्मों, बस अड्डों और वेश्यालयों के बाहर रात गुजारने वाले मजदूरों के संघर्ष को हमेशा सलाम किया है, क्योंकि मुंबई को सजाने और चमकाने में मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह सच है कि मुंबई की जान मेहनतकशों की बस्ती में बसी है।
(प्रकाशित)



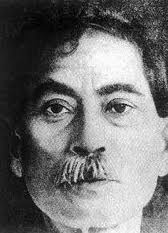
Comments
Post a Comment